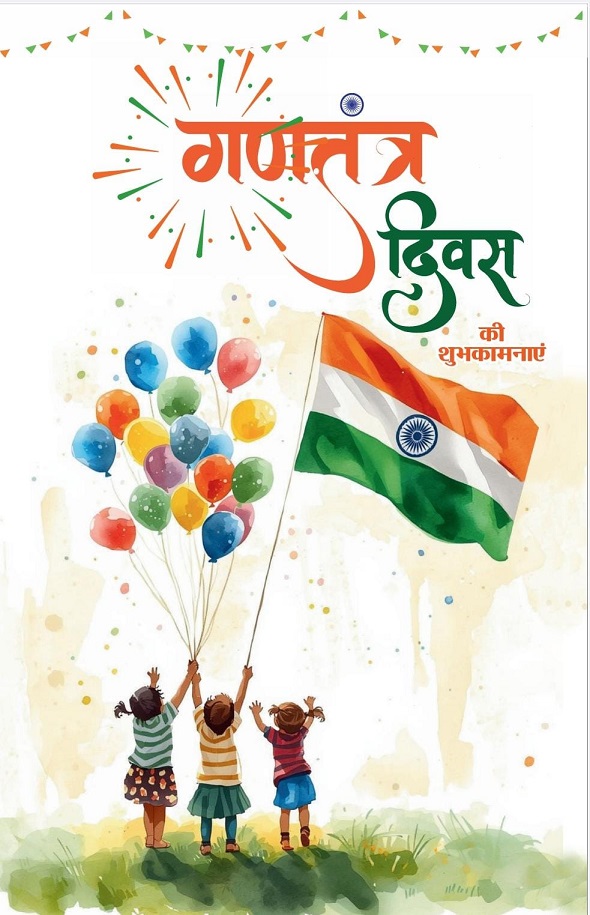कह सकते हैं कि बाजार ने हिंदी को विस्तार दिया है। बिल्कुल ऐसा हुआ है। लेकिन बाजार में वह विनिमय की भाषा के रूप में स्थापित हुई है। लेकिन बाजार को संचालित करने वाली ताकतों की भाषा अब भी हिंदी नहीं है। यह कुछ बालीवुड जैसा ही है।
आर्थिक व्यवस्था और संस्कृति के संदर्भ में भी हमें यह मानने से गुरेज नहीं होना चाहिए क िअपना देश विरोधाभासों का देश है। राष्ट्र के भाषायी सोच के संदर्भ में भी हमें रोजाना इस विरोधाभासी अंदाज से दो-चार होना पड़ता है। एक तरफ देश का एक बड़ा तबका अपनी हिंदी को लेकर स्वाभिमानी अंदाज में आगे बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ एक बड़ा तबका इस सोच को ही नकार रहा है। विविधताओं में एकता का संदेश हमें बचपन से ही घुट्टी में मिला है। सरकारें चाहे जिस भी विचारधारा की हों, लेकिन उन्होंने पाठ्यक्रमों में स्थित इस सोच को कभी हटाया नहीं। इसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि कम से कम भाषा के स्तर पर इस एकता राग को राष्ट्र स्वीकार नहीं कर पाया है? विश्व हिंदी दिवस, इस मुद्दे पर गहन सोच-विचार का अच्छा मौका हो सकता है।
राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बहाने चाहे जितने भी सरकारी प्रयास हुए हों, लेकिन भारत का हर हिस्सा हिंदी को लेकर कम से कम उस तरह नहीं सोच पाया है, जैसा उन्नीसवीं सदी के आखिर में बंगला और गुजराती मूल की हस्तियों ने सोचा था। 1857 की नाकामी के बावजूद तब देश में यह सोच बलवती हो चुकी थी कि अंग्रेजी दासतां से उसे मुक्ति मिलनी ही है। तत्कालीन मानस यह भी मान चुका था कि अंग्रेजी शासन से मुक्ति के बाद जो राष्ट्र होगा, वह कम से कम तब तक के मौजूद राजनीतिक ढांचे से अलग हो। तब समाज के प्रबुद्ध लोग मान चुके थे कि आजाद भारत सिर्फ सांस्कृतिक रूप से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक होगा।
इसी संदर्भ में विविधरंगी और बहुभाषी भारत की एक ऐसी भाषा की कल्पना भी जन्म लेने लगी, जो समूचे राष्ट्र की संपर्क भाषा बन सके। समूचे राष्ट्र की हिंदी ही संपर्क भाषा हो सकती है, पहली बार यह विचार 1875 में केशवचंद्र सेन ने दिया। यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि ठीक उन्हीं दिनों देश के पश्चिमी सिरे यानी गुजरात में भी ऐसी ही सोच पल्लवित हो रही थी। गुजराती के कवि नर्मदाशंकर ने 1882 में हिंदी को लेकर कुछ वैसा ही विचार दिया, जैसा केशवचंद्र सेन का था। गुजराती समाज उन्हें नर्मद कवि के रूप में जानता है। भावी भारत की भाषा को लेकर देश के सुदूर पूर्वी इलाके से लेकर सुदूर पश्चिमी इलाके तक में एक जैसी सोच चकित करती है। क्योंकि तब आज की तरह संचार के साधन नहीं थे। मीडिया भी नहीं था। ऐसे में पूरब और पश्चिम की सोच में एक-दूसरे पर संपर्क के जरिए असर पडऩे का सवाल भी नहीं उठता। बाद के दिनों में चाहे तिलक महाराज हों या फिर गांधी, काका कालेलकर हों या विनोबा, उन्होंने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए हिंदी को जो चुना, उसकी बुनियाद उन्नीसवीं सदी के आखिर में उभरा विचार ही रहा।
आजादी के आंदोलन में गांधी ने हिंदी के प्रसार को जोड़कर जो उंचाई दी, उससे उम्मीद थी कि स्वाधीनता के बाद केशवचंद्र सेन और नर्मदकवि की सोच साकार हो उठेगी। ऐसा हुआ भी, लेकिन विरोधाभासों के साथ। दक्षिणी राज्यों मसलन कर्नाटक और तमिलनाडु में हिंदी को वैसी सहजता से स्वीकार नहीं किया जा सका, जैसा दूसरे राज्यों ने स्वीकार कर लिया है। वैसे यह बात और है कि जब कर्नाटक या तमिलनाडु का व्यक्ति विंध्य के उत्तर में आता है तो यह मानकर आता है कि सहज कार्यव्यवहार के लिए उसे हिंदी जानना ही होगा। दक्षिण लौटते ही अगर वह अपनी भाषा में फिर लौट जाता है तो यह उसका अधिकार है। ऐसा होना सहज भी है। लेकिन वह इससे आगे बढ़ जाता है। हिंदी को लेकर उसका रवैया बदल जाता है। स्थानीय राजनीति इसे बढ़ावा भी देती है। स्थानीय राजनीति के लिए उनकी अपनी स्थानीय भाषाएं राजनीतिक औजार बन गई हैं। इस औजार के जरिए वे अपना लक्ष्य यानी वोटर का समर्थन चाहती हैं और उन्हें मिलता भी है।
वर्धा में 10 जनवरी 1974 को हुए पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का घोषित लक्ष्य हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाना रहा। लेकिन अघोषित लक्ष्य हिंदी को भारत की जनगण की भाषा भी बनाना था। भले ही वह द्वितीयक भाषा बने। हमारा केंद्रीय राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र भले ही दस जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की ओर आगे बढ़ चुका हो, लेकिन उसका मानस अभी हिंदी को लेकर सहज नहीं हो पाया है। मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व के दौर में हिंदी को लेकर देश के स्टील फ्रेम यानी नौकरशाही का रवैया बदला तो है, लेकिन वह बेहद अत्यल्प है। अब भी वह विदेशी भाषा में सोचता है, नीतियों का निर्माण भी करता है। हिंदी बेचारी अब भी उनकी नजर में अनुवाद की भाषा है।
कह सकते हैं कि बाजार ने हिंदी को विस्तार दिया है। बिल्कुल ऐसा हुआ है। लेकिन बाजार में वह विनिमय की भाषा के रूप में स्थापित हुई है। लेकिन बाजार को संचालित करने वाली ताकतों की भाषा अब भी हिंदी नहीं है। यह कुछ बालीवुड जैसा ही है। संचार क्रांति के पहले हिंदी के प्रसार के लिए सिनेमा की खूब बलैया ली जाती थीं। लेकिन यह भी कटु सत्य रहा कि बॉलीवुड को संचालित करने वाले तंत्र की भाषा हिंदी नहीं रही। इसलिए बाजार के जरिए हिंदी के विकास की सोच को लेकर ज्यादा इठलाने की जरूरत नहीं है। बाजार या सिनेमा के जरिए भाषा का प्रसार तो हो सकता है, लेकिन उसे ताकत नहीं मिल सकती। उसे ताकतवर तो क्षमतावान लोगों द्वारा संचालन और नियंत्रण की भाषा के रूप में उसका व्यवहार बनाता है।इसे हमें स्वीकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि हिंदी अब भी वह सम्मान नहीं हासिल कर पाई है। वह संचालकों, नियंत्रित करने वाले कारकों, नीति नियंताओं, विमर्शकारों की भाषा नहीं बन पाई है। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर अगर जिम्मेदार लोग ऐसे संकल्प लें कि वे इसे विमर्श का माध्यम बनाएंगे, नीति निर्माण में देसज सोच को महत्ता मिलेगी, संचालन प्रक्रिया में हिंदी का प्रयोग होगा, तभी हिंदी के लिए ऐसे दिवस मनाना सार्थक हो सकेगा। सवाल यह है कि क्या इस तरीके से हम हिंदी वाले, हमारे नियंता और हमारे विमर्शकार सोचने को तैयार हैं।